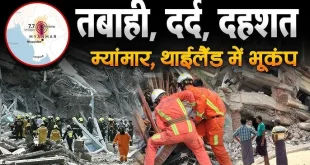सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबरों पर सक्रिय हो गया है। इस मामले की जांच के लिए तीन जजों की एक समिति गठित की गई है। जस्टिस वर्मा ने इस समिति के सामने पेश होने से पहले पांच वकीलों से कानूनी सलाह ली है।
क्या जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है?
इस सवाल के जवाब में 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि वे भी लोकसेवक की श्रेणी में आते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जज भी जवाबदेह हैं। हालांकि, भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अनुमति आवश्यक होती है।
एफआईआर के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी
सीआरपीसी के अनुसार, पुलिस संज्ञेय अपराध के मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन जजों के मामले में विशेष प्रावधान लागू होते हैं। किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य होती है, जो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही दी जा सकती है।
जस्टिस वर्मा मामले में ताजा घटनाक्रम
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जस्टिस वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी मिलने के सबूत, फोटो और वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा किए हैं। हालांकि, अभी तक सरकार ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर मुख्य न्यायाधीश से औपचारिक सलाह मांगी है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
1991 का ऐतिहासिक फैसला और उसका प्रभाव
यह मामला हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के. वीरास्वामी से जुड़ा है, जिनके खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिटायरमेंट के डेढ़ महीने बाद मामला दर्ज किया था। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जजों को कानूनी संरक्षण केवल इसलिए दिया गया है ताकि वे स्वतंत्र रूप से न्याय कर सकें और सरकार से कोई प्रतिशोध न हो। लेकिन यदि भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलते हैं, तो चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति की अनुमति से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है।
क्या महाभियोग की जरूरत पड़ेगी?
संविधान के अनुसार, किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना आवश्यक होता है। प्रस्ताव को दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित करना जरूरी होता है। अब तक भारत में तीन मौकों पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन किसी भी जज को हटाया नहीं गया। तीनों मामलों में संबंधित जजों ने महाभियोग प्रस्ताव पारित होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।
1991 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जज भी एक लोकसेवक हैं और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम महत्वपूर्ण होगा।
 News India Live | Breaking India News,The Indian Headline,India Express News,Fast India News The Hindu,Hindustan Times
News India Live | Breaking India News,The Indian Headline,India Express News,Fast India News The Hindu,Hindustan Times